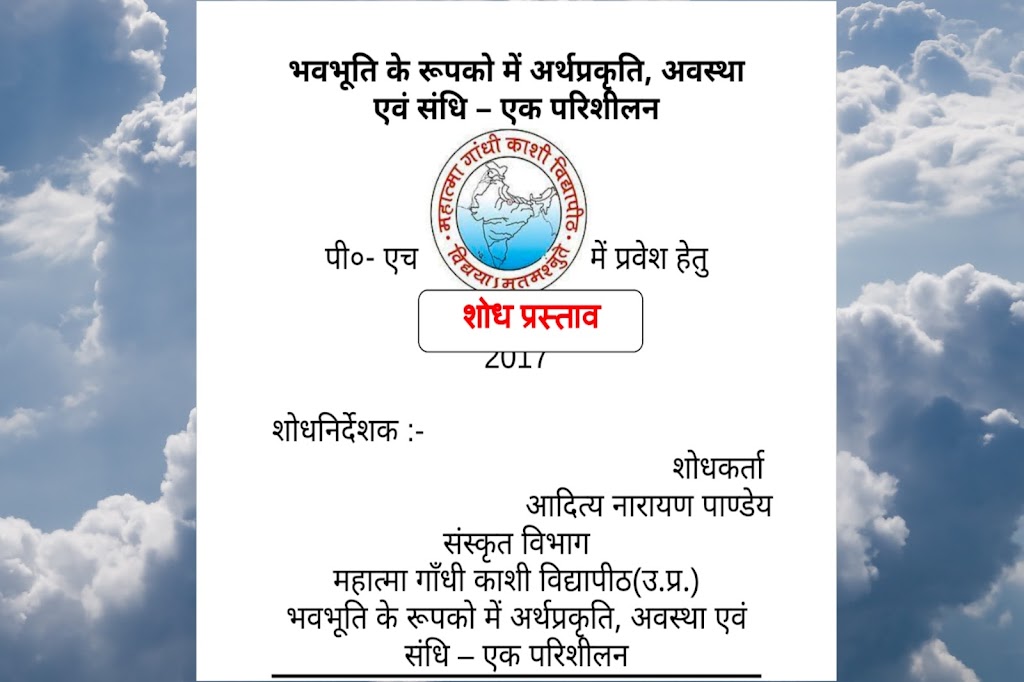शोध प्रबंध के रूपरेखा
भवभूति के रूपको में अर्थप्रकृति, अवस्था एवं संधि – एक परिशीलन
पी०- एच० डी० (संस्कृत) में प्रवेश हेतु
2017
शोधनिर्देशक :-
शोधकर्ता
आदित्य नारायण पाण्डेय
संस्कृत विभाग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ(उ.प्र.)
भवभूति के रूपको में अर्थप्रकृति, अवस्था एवं संधि – एक परिशीलन
भूमिका :-
संस्कृत साहित्य भारतवर्ष के आत्मतत्व का प्रतीक है | अति प्राचीनकाल में प्रवाहमान इस साहित्यधारा में यहां के मनीषियों एवं रचना कार्य की भावनाओं, कल्पनाओं एवं आकांक्षाओं की प्रतिछवि सजीव रूप से दृष्टिगोचर होती है | संस्कृत साहित्य की यह परंपरा वैदिक काल से लेकर अध्यावधि पर्यंत अनवरत रूप से विकसित होती रही है | अपनी संपन्नता तथा विविधता में यह साहित्य विश्वाअंगमय में अद्वितीय है | संस्कृतकाव्य में संस्कृत महाकवियो की कोमल कल्पना तथा सरसता का कोई प्रतिमान नहीं है | संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों द्वारा काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है | प्रथम दृश्य एवं द्वितीय श्रव्य-
Read more – meghdoot
“ दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुन: काव्यं द्विधा मतम् |”
(साहित्यदर्पण) षष्ठ परिच्छेद
साहित्य दर्पणकार द्वारा प्रतिपादित काव्य के उपर्युक्त विभाजन में दृश्य काव्य का अपना विशिष्ट महत्व है | क्योंकि इसके अंतर्गत परिगणित रुपको एवं उपरूपकों का रसास्वादन जनसामान्य की स्रोत एवं चक्षु दोनों के द्वारा होता है | यही कारण है कि काव्य वेदों में रूपक या नाटक की रमणीयता की प्रशंसा की गई है |
गर्भ संधि :-
पताका और प्रत्याशा को मिलाकर गर्भ संधि का निर्माण होता है | तथा जहां पताका ना हो वहां पर प्रत्याशा पर ही अवलंबित रहती है |
विमर्श संधि :-
प्रकरी और नियताप्ति को मिलाकर बिमर्श – संधि इनको ही अवमर्श संधि भी कहते हैं | जहां प्रकरी न हो वहां नियताप्ति पर ही निर्भर रहती है |
उपसंहृति संधि :-
कार्य और फलागम को मिलाकर उपसंहृति संधि इसको ही निर्वहण संधि भी कहते हैं | संधियों को कथा का स्थूल भाग कहा जा सकता है | इनके आधार पर ही नाटक का विभाजन किया जाता है अतः प्रसिध्द रूपककार भवभूति के अपने नाटकों में यथास्थान अर्थप्रकृति अवस्था एवं संधि का विवेचन किया है |
Read more – varn vichar
शोध प्रबंध की प्रस्तावित रूपरेखा :-
अध्याय विभाजन
- प्रथम अध्याय – भवभूति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व
- द्वितीय अध्याय – रूपकों का संक्षिप्त परिचय
- तृतीय अध्याय – रूपकत्रय अर्थप्रकृति विवेचन
- चतुर्थ अध्याय – रूपकत्रय में अवस्था विवेचन
- पंचम अध्याय – रूपकत्रय में संधि विमर्श
- षष्टम अध्याय – अर्थप्रकृति, अवस्था एवं संधि का वैशिष्ट्य उपसंहार
परिशिष्ट –
उद्धृत वाक्य सूची
संदर्भ ग्रंथ सूची
”काव्येषु नाटकं रम्यम् |”
संस्कृत नाट्यरचना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है | ईसा पूर्व लगभग 500 वर्ष पूर्व विद्वान महाकवि विभास की नाटक रचनाएं नाट्यसाहित्य में उपलब्ध वर्तमान में सर्वप्राचीन है | महाकवि भास के परवर्ती रूपकारों में कालिदास शूद्रक अश्वघोष एवं भवभूति आदि प्रमुख है | इनमें से भवभूति अपनी विशिष्ट नाट्य शैली एवं अद्भुत कल्पना कौशल के कारण संस्कृत साहित्य में अपना अप्रतीम स्थान रखते हैं |
Read more- Kalidas ka jivan Parichay
महाकवि भवभूति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व :-
संस्कृत साहित्यकाश के देदीप्यमान नक्षत्र महाकवि भवभूति के विषय में उनकी तीनों नाट्यकृतियों की प्रस्तावना में प्रदत सामग्री (विवरण) के आधार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | तदनुसार उनके पूर्वज पदमपुर नगर के निवासी थे | वे काश्यपगोत्र के यजुर्वेद के तैत्रियशाखा के पंक्ति पावन ब्राह्मण थे | इनके दादा का नाम भट्टगोपाल तथा पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकरणी या जातुकरणी था |
श्रीकंठ इनकी उपाधि थी | जगध्दर आदि कुछ टीकाकारों की मान्यता है कि श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम था, तथा एक श्लोक में भवभूति शब्द का चमत्कार पूर्वक प्रयोग के कारण इन्हें भवभूति की उपाधि मिली |
सीमांकन :-
इस शोध कार्य हेतु केंद्र बिंदु रूप में मुख्यता अधोदभ ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा |
- नाट्यशास्त्र
- दशरूपक
- साहित्यदर्पण
- मालतीमाधवम् (प्रकरण)
- महावीरचरितम्
- उत्तररामचरितम्
शोध विधि :-
इस शोध कार्य की आवश्यकता के अनुसार इसमें वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक इन तीनों शोध विधियों का उपयोग किया जाएगा |
श्रीकंठपदं लाछनं नाम यस्य स: |
पितृकृतनामेगम् (महावीर चरित्र वीर राधव कृतटीका)
कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा का आश्रय महाकवि भवभूति को प्राप्त था | महाकवि भवभूति विरचित तीन रूपक प्राप्त होते हैं |
- मालतीमाधवम् (प्रकरण)
- महावीरचरितम्
- उत्तररामचरितम्
उपर्युक्त तीनों रचनाओं में महाकवि भवभूति के उत्कृष्ट नाट्यकला का दिग्दर्शन होता है | अपनी कल्पना कौशल शास्त्रीय पांडित्य सूक्ष्म सर्वेक्षण दृष्टि और अलौकिक प्रतिभा के बल पर भवभूति ने नाट्य रचना संसार में अपना अप्रतिम स्थान सुनिश्चित किया | उत्तररामचरितम् भवभूति के नाटक कौशल का चुडान्तनिदर्शन है | करुण रस प्रधान इस सप्तांकात्मक नाटक का कोई प्रतिमान नहीं है |
भवभूति के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उन में प्रयुक्त नाट्यतत्वों का उचित एवं पूर्ण सन्निवेश है | कथानक की सजीवता पात्रों की चरित्रांकन भाषा का प्रवाह एवं रस की अवैधता के साथ-साथ नाट्य के मूल्य तत्वों – अर्थप्रकृति कर्यावस्था संधि अर्थोक्षेपक आदि का भी समुचित प्रयोग उनके नाट्य शास्त्रीय ज्ञान का सूक्ष्म रचना दृष्टि को प्रकट करता है |
अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभि: |
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमा: | | (धनञ्जयकृत दशरूकम्) |
फल की कामना करने वाले व्यक्तियों (नायक आदि) के द्वारा प्रारम्भ किये गए कार्य की पांच अवस्थाये – (1) आरम्भ (2) यत्न (3) प्राप्त्याशा (4)नियताप्ति (5)फलागम होती है |
आरंभ :–
मुख्य फल की सिद्धि / अत्यधिक फल की प्राप्ति के लिए नायक में जो उत्सुकता होती है उसे आरंभ कहते हैं |
यत्न :-
फल की प्राप्ति के लिए नायक बड़े बेग से जो प्रयत्न करता है उसे यत्न कहते हैं |
प्रत्याशा :-
जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना होती है और विघ्नों के कारण वह असंभव दिखती है | उस संदिग्ध अवस्था को प्रत्याशा कहते हैं |
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श (विमर्श) और उपसन्हृति अर्थात निर्वाहण नामक पांच संधियां हैं |
अर्थप्रकृति + अवस्था = संधि
बीज + प्रारंभ = प्रतिमुखसंधि |
बिंदु + प्रयत्न = प्रतिमुख्यसंधि |
पताका + प्रप्त्याशा = गर्भ संधि |
प्रकरी + नियताप्ति = अवमर्श सन्धि |
कार्य + फलागम = निर्वहण (उपसंहृति) संधि |
मुख संधि :-
बीज और आरंभ को मिलाकर मुख – संधि होती है |
प्रतिमुख संधि :-
बिन्दु और यत्न को मिलकर प्रतिमुख संधि का निर्माण होता है तथा जहां पताका ना हो, वहां पर प्रत्याशा पर ही अवलम्बित रहती है |
भवभूति के रूपको में अर्थप्रकृति/अर्थप्रकृति निरूपण :-
अर्थ प्रकृति का अर्थ धनंजय और विश्वनाथ अर्थप्रकृति का अर्थ किया है
“प्रयोजनसिध्दिहेतव:” अर्थात जो प्रायोजन की सिद्ध में कारण हो |अर्थप्रकृतियाँ नाटकीय कथावस्तु में पांच तत्व है, जो निम्नवत है | लक्षण :-
“ बीजबिंदुपताकाव्य प्रकरीकार्य लक्षणा: |
अर्थप्रकृतय पञ्च ता एता परिकीर्तिता: | |” (धंनजयकृत दशरूपकम्)
(i)बीज :-
यह तत्व है जो वृक्ष के बीज की तरह प्रारंभ में संक्षेप में निर्दिष्ट हो और आगे उसका ही अनेक प्रकार से विस्तार हो | यह नायक के मुख्य फल का कारण होता है | उ० भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह बीज है|
(ii) बिन्दु :-
अवान्तर कथा से मूल कथा के टूट जाने पर जो उसे जोड़ता है, और आगे बढ़ाता है, उसे बिंदु कहते हैं |
नियताप्ति:-
जब विघ्नों के हट जाने के कारण फल की प्राप्ति निश्चित जान पड़ती है उस अवस्था को नियताप्ति कहते हैं |
फलागम :-
जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है उस अवस्था को फलागम कहते हैं |
भवभूति के रूपको में संधियों का निरूपण :-
पांच अवस्थाओं का निर्देशन कर चुकने के पश्चात्त अब पांच संधियों का विवेचन करते हैं |
संधि का अर्थ :-
दो भागों का मिलना ही संधि है पांचों अर्थ प्रकृतियों को पांचो अवस्थाओं में जो संबंध करती है उन्हें संधियाँ कहते हैं | ये अर्थप्रकृति से अवस्था का संबंध करती हैं |
लक्षण :-
“ मुखप्रतिमुखे गर्भ: शावमर्शोपंसहृति: |” (दशरुपकम्)
समस्या कथन :-
महाकवि भवभूति के रूप कसरत की उत्कृष्टता का सर्वप्रमुख कारण उनमें नेतृत्व की समुचित समन सन्निवेश है भूत ने अपने समस्त रचनाओं में नाटक तत्वों का यथोचित प्रयोग किया है उनकी रचनाओं में प्रमुख किन स्थानों पर प्रकृति अर्थव्यवस्था एवं संदेश किया है इसके लिए एक नवीन अनुसंधान की आवश्यकता है संस्कृत काव्य महाकवि भवभूति की नाटक अत्यंत सम्मानीय उत्कृष्टता से युक्त है उनके नाट्य कौशल की प्रशंसा सूजी समीक्ष जन मुक्तकंठ से करते हैं अतः शोधार्थी का उद्देश्य भभूत के रूप को में विद्यमान प्रमुख नाट्य तत्व अर्थ प्रकृति कार्य अवस्था एवं संधि का सूक्ष्म शिक्षण करते हुए इनके समावेश के औचित्य एवं उपर्युक्त कोशिश करने का प्रयास करना है |
शोधोद्देश्य : –
संस्कृतसाहित्य में महान कवि भवभूति की नाट्य कला अत्यन्त सम्माननीय एवं उत्कृष्टता से युक्त है | उनके नाट्य कौशल की प्रशंसा सुधि समीक्षक जनमुक्त कंठ से करते आ रहे है | अत: शोधार्थी का उद्देश्य भवभूति के रुपको में विद्यमान प्रमुखनाट्यतत्वों अर्थप्रकृति कार्यवस्था एवं संधि का सूक्ष्म समीक्षण करते हुवे इनके समावेश के औचित्य एवं उपयुक्तिता को सिध्द करने का प्रयास करना है |
पताका :-
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है | जैसे – सुग्रीव आदि का वृतांत |
प्रकरी :-
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर चलती है | जैसे – रामायण में शबरी की कथा
कार्य :-
कार्य का अर्थ फल है जिस फल की प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है | जो साध्य होता है वह कार्य है | जैसे – रामायण में रावण का वध |
यह फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, में से कोई भी हो सकता है इसको ही मुख्य प्रयोजन, लक्ष्य आदि कहते हैं |
भवभूति के रूपकों में अवस्थाएं / अवस्था निरूपण कार्य की पांच अवस्थाएं :-
पांच अर्थप्रकृतियों का निर्देश कर चुकने के पश्चात अब ग्रंथकार (नाटक की) कार्य की पांच अवस्थाओं का विवेचन करते हैं