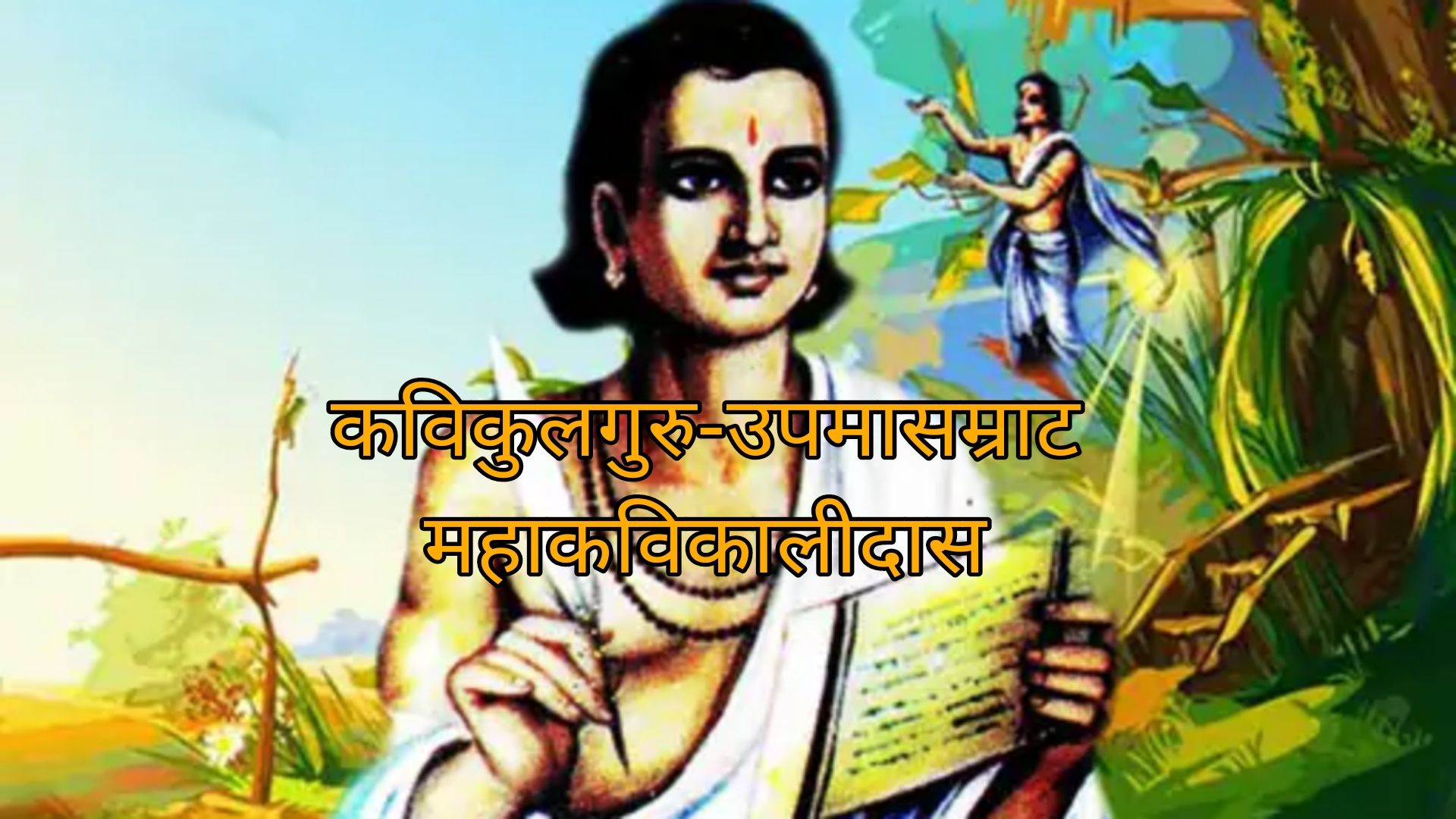कालिदास
महाकवि कालिदास सरस्वती के अमर पुत्र तथा सुरभारती के सनातन श्रृंगार हैं। केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु विश्व-साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। उनका साहित्य एक ऐसी अनुपम रत्न-राशि है, जिसमें से भाषा, भाव तथा कल्पना के अमूल्य रत्नों को लेकर परवर्ती साहित्यकारों ने अपनी कला को अलंकृत तथा काव्य-सम्पदा को समृद्ध बनाया है। क्या देशी क्या विदेशी सभी विद्वानों एवं कवियों ने इस रससिद्ध कवीश्वर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
जर्मन के विद्वान ने कालीदास के बारे में कहा-
‘वसंतं कुसुमं फलं च युगपद् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत्
यच्चान्यनमनसो रसायनमतः सन्तपर्ण मोहनम्। एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो-
रैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे ! शाकुंतलं सेव्यताम्।।’
भावार्थ –
‘क्या तू उदीयमान वर्ष के पुष्प और क्षीयमाण वर्ष के फल देखना चाहता है ? क्या तू वह सब देखना चाहता है, जिससे आत्मा मन्त्रमुग्ध, मोदमग्न, हर्षाप्ला- वित और परितृप्त हो जाती है? क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी का एक हो जाना पसन्द करेगा ? अरे, तब मैं तेरे समक्ष ‘शाकुन्तल’ को प्रस्तुत करता हूँ और बस सब कुछ इसमें आ गया।
‘निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु।
प्रीतिर्मधुरसंद्रासु मंजरीश्विव जायते।।’
किसी रसिक ने अपना अभिमत प्रकट किया है :-
‘पुरा कविनां गणनाप्रसङ्गे
कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः।
अद्यपि तत्तुल्यकवेरभावा –
दनामिका सार्थवती बभूव।।
इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक सभी विद्वानों ने कालीदास का हृदय खोलकर समादर किया है।
कालिदास का जीवन – परिचय:-
संस्कृत के अन्य कवियों से हटकर कविवर कालिदास ने अपने जीवन के सम्बन्ध में वस्तुतः कुछ भी नहीं लिखा । एक जनश्रुति बतलाती है कि जीवन के पूर्वकाल में वे महामूर्ख थे। उनका विवाह विद्योत्तमा नामक एक राजकुमारी से हो गया। उनकी मूर्खता से क्रुद्ध होकर राजपुत्री ने उन्हें घर से निकाल दिया। उसके उपरांत सरस्वती की आराधना करके उन्होंने कवित्व-शक्ति प्राप्त की और घर लौटकर पत्नी से प्रवेश के लिए प्रार्थना की । कौन है ? – यह पूछे जाने पर अपनी विदुषी भार्या को आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने शुद्ध संस्कृत में उत्तर दिया- ‘अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः’ । पश्चात् पूर्ण जानकारी के बाद पत्नी ने द्वार खोला।
कालिदास ने ‘अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः’ के ‘अस्ति’ पद से कुमारसम्भव महाकाव्य लिखा- अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः’ ।
‘कश्चित्’ पद से मेघदूत की रचना की ‘कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः’ ।
‘वाग्’ शब्द से रघुवंश महाकाव्य लिखा- ‘वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रति- पत्तये’ ।
Read more– Maheshwar Sutra
इसी भाँति एक दूसरी किंवदन्ती के अनुसार कालिदास लंका के राजा कुमारदास के मित्र कहे जाते हैं। कहते हैं कि एक बार वे कुमारदास से मिलने लंका गए थे, जहाँ लालची वेश्या द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।
एक तीसरी जनश्रुति के अनुसार कालिदास महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। विक्रम के नवरत्नों के नाम इस प्रकार बताये गए हैं:-
‘धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशङ्कु-
वेतालभट्टघटखर्परकालिदासः।
‘ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभयां
रत्नानि वं वररुचिर्नवविक्रमस्य।।
(ज्योतिर्विदाभरण)
कालिदास की जन्म-भूमि:-
महाकवि कालिदास ने अपने जन्म से किस भू-भाग को अलंकृत किया, यह भी मतभेद का विषय है। महाकवि ने; कण्वाश्रम, वशिष्ठाश्रम तथा अलकापुरी के बड़े ही मनोहारी वर्णन किये है-इत्यादि तकों के आधार पर कुछ लोग इनको कश्मीर निवासी मानते हैं।
कुछ विद्वान् इन्हें काली का उपासक मानकर मिथिला को इनकी जन्म-भूमि सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि दरभंगा जिले में उच्चैठ नामक स्थान में, जहाँ अभी भी भगवती काली का मन्दिर विद्यमान है, यही कालिदास को सिद्धि प्राप्त हुई थी। कालिदास कुमारसम्भव के आठवें सर्ग में लिखा है कि विवाह के उपरान्त महादेव जी अपनी ससुराल में एक मास तक रहे- “शैलराजभवने सहोमया मासमात्रमवसद् वृषध्वजः”।
यह बात आज भी मिथिला में ही पायी जाती है कि वहाँ वर को विवाह-यात्रा में एक मास तक रखने के बाद विदा किया जाता है। इस प्रकार महाकवि ने मिथिला की कई ऐसी बातों का वर्णन किया है, जो वहाँ का निवासी ही कर सकता है।
किन्तु अधिकांश विद्वान् कालिदास को मालवा प्रदेश निवासी मानते हैं। वे कहते है कि कालिदास ने जिस आत्मीयता के साथ उज्जयिनी का वर्णन किया है। उससे महाकवि की जन्मभूमि उज्जयिनी अथवा उसके आस-पास कहीं अवश्य रही होगी।
कालिदास की काव्यकला:-
कालिदास की भाषा और शैली:-
कालिदास के ग्रन्थ:-