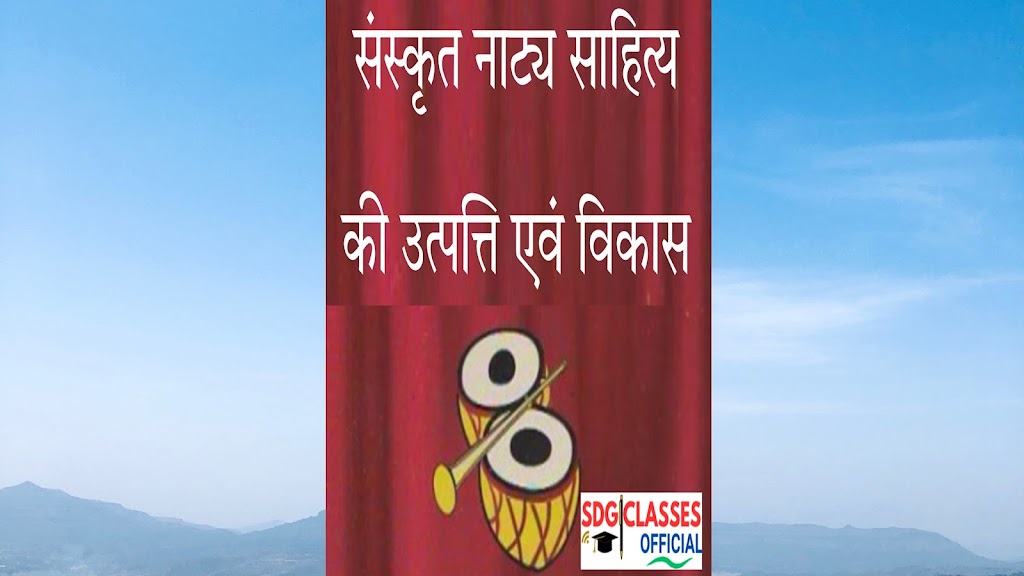संस्कृत नाट्य साहित्य की उत्पत्ति एवं विकास
कथा और आख्यायिका –
संस्कृत नाट्य साहित्य में कथा और आख्यायिका के नाम से कथा साहित्य का विपुल भंडार है। इन दोनों विधाओं में मूल तत्व एक ही है। अंतर केवल एक ही है प्रस्तुतीकरण का। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कथाकार दंडी ने कथा और आख्यायिका में अंतर बताते हुए लिखा है कि कथा में नायक या उससे भिन्न किसी भी पत्र के द्वारा कथा कही जा सकती है। जबकि आख्यायिका में स्वयं नायक ही सम्पूर्ण कथा को कहता है।
कहानी की उत्पत्ति –
संस्कृत कहानी के बीज विश्व के सबसे प्राचीनतम् ग्रन्थ ऋग्वेद के दसवें मंडल की कथाओं में मिलते हैं। ऋग्वेद की वही कथाएँ बाद के उपनिषदों, पुराणों, ब्राह्मणों और अरण्यकों में विकसित होकर कथा की पृष्ठभूमि तैयार करती रहीं। इसके बाद यह परंपरा मूल काव्य रामायण और महाभारत में भी जारी रही। इन सभी ग्रन्थों में विभिन्न कहानियों का वर्णन पद्यरूप में किया गया है, जबकि आधुनिक कहानी का रूप गद्य है।
वैदिक साहित्य के पश्चात् लौकिक गद्य ने पर्याप्त विकास किया और उसमें अनेकानेक रचनाएँ की गई, किन्तु दुर्भाग्य से वे काल-कवलित हो गईं। वर्तमान में उपलब्ध उत्कृष्ट गद्य साहित्य की परम्परा हमें दण्डी, सुबन्धु एवं बाण आदि की रचनाओं में देखने को मिलती है। इन सभी के गद्य में कथा और आख्यायिका के रूप में अनेकानेक कथाएँ सन्निहित हैं। संस्कृत भाषा के परिवर्तित रूप पालि एवं प्राकृत भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में कथा-साहित्य की रचना की गई। इनमें बौद्ध-साहित्य की जातक कथाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है
Read more – Meghdoot shlok 21 to 25
कथा-साहित्य के दो रूप-
संस्कृत कथा-साहित्य को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- महाकथा, लघु-कथा।
महाकथा –
महाकथा से यहाँ हमारा आशय उपन्यास जैसी लम्बी कथाओं से है। महाकवि दण्डी की ‘दशकुमारचरितम्’ और ‘अवंतीसुन्दरी कथा’; सुबन्धु की ‘वासवदत्ता’; बाणभट्ट की ‘हर्षचरितम्’ और ‘कादम्बरी’; विश्वेश्वर पांडे की ‘मंदारमंजरी’; पंडित अम्बिकादत्त व्यास द्वारा लिखित ‘शिवराजविजयः ‘हृषिकेश शास्त्री पट्टाचार्य द्वारा ‘प्रबंधमंजरी’; पंडिता क्षमाराव द्वारा लिखित ‘कथामुक्तावली’; मेघव्रताचार्य कृत ‘कुमुदिनीचन्द्रम्’; धनपाल कृत ‘तिलकमंजरी’; वादिभासिंह कृत ‘गद्यचिन्तामणि’ आदि इसी श्रेणी की संस्कृत-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं।
लघु-कथा –
इन कथाओं के अन्तर्गत छोटी-छोटी कथाओं को समाहित किया गया है। इनको भी दो भागों में बाँटा जा सकता है- (क) नीति-कथा, (ख) लोक-कथा।
(क) नीति कथाएँ –
इन कहानियों में रीति-रिवाज, नीति, कर्तव्य, अकर्तव्य और जीवन मूल्यों से संबंधित बातों को समझना सिखाया जाता है; इसलिए इन्हें उपदेश कंठ भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में ‘पंचतंत्र’ और ‘हितोपदेश’ सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके अलावा संस्कृत साहित्य में प्रचलित अनेक नीति-कथा सम्बन्धि ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।
पंचतंत्र :-
इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। महिलानरोप्य नगर के राजा अमरशक्ति के मूर्ख पुत्रों को शास्त्रज्ञ और कुशल बनाने के लिए उन्होंने इस कथा-ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने पशु-पक्षियों को पात्र बनाकर नैतिक कहानियाँ लिखी हैं। इसके पाँच तंत्र हैं:
(1) मित्र-मतभेद
(2) मित्र-सम्प्राप्ति
(3) संधि संघर्ष
(4) लब्ध प्रणाम
(5) अपरीक्षित कारक।
इसीलिए इसे ‘पंचतंत्र’ कहा जाता है आज पंचतंत्र की कहानियों का दुनिया की 250 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है; इसलिए विश्व कथा साहित्य में इसका सर्वोच्च स्थान है। इसकी रचना तिथि अभी भी अनिर्णीत है।
हितोपदेश :-
‘पंचतंत्र’ के बाद ‘हितोपदेश’ को कथा साहित्य में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं।इसमें कुल 43 कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें से 25 पंचतंत्र से ली गई हैं। इस में ‘पञ्चतन्त्रम्’ के तन्त्रों के स्थान पर चार परिच्छेद हैं- मित्र-लाभ, सुहद-भेदः विग्रह और सन्धि। इसका रचना-काल १३०० ई० माना जाता है।
(ख) लोक-कथा –
संस्कृत की लघुकथाओं में दूसरा रूप लोक कथाओं का है। इनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना रहा है और उनके कथानक लोक-अवधारणाओं पर आधृत होते हैं. इसीलिए इन्हें मनोरंजन कथा, लोक कथा एवं दन्त-कथा के नाम से भी जाना जाता है। इनके अधिकांश पात्र मनुष्य ही हैं। संस्कृत-साहित्य की अत्यन्त प्रसिद्ध प्रमुख लोक-कथाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-
बृहत्कथा –
इसकी रचना गुणाढ्य ने प्राकृत भाषा में की थी। इसका रचनाकाल ईसा की द्वितीय शताब्दी माना जाता है। आज यह मूल रूप में प्राप्त नहीं है. किन्तु इसकी कथाओं पर आधारित संस्कृत में चार कथा-ग्रन्थ उपलब्ध है ।
(1) बृहत्कथा श्लोक संग्रह –
ईसा की आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रचित पद्यमय रचना है। इसके रचयिता बुद्ध स्वामी है।
(2) बृहत्कथा कोश –
सन् 932 ई० में रचित यह गद्य- पद्य मिश्रित कथा-संग्रह है। इसमें 1250 श्लोक एवं 157 कथाएँ सङ्कलित हैं। इसके रचनाकार हरिषेण हैं।
(3) बृहत्कथा मञ्जरी –
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में रचित इस रचना में 7500 श्लोक हैं। इसके रचनाकार महाकवि क्षेमेन्द्र हैं।
(4) कथासरित्सागर –
यह भी ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की रचना है। इसमें 18 खण्ड तथा 24 उपखण्ड हैं। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि सोमदेव भट्ट हैं।.
बेतालपञ्चविंशतिका –
ईसा की बारहवीं शताब्दी में शिवदास रचित यह संस्कृत का अतिप्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ है। इसमें कुल 25 कथाएँ हैं, जिनको वेताल राजा त्रिविक्रमसेन को सुनाता है। यद्यपि इसका मूलरूप आज प्राप्त नहीं है। इसका वर्तमान में उपलब्ध संस्करण बारहवीं शताब्दी का है।
शुकसप्तति –
यह 70 कथाओं का कथा-ग्रन्थ है और इनका वक्ता शुक अर्थात् तोता है। ईसा की ग्यारहवी शताब्दी की इस रचना के रचयिता का नाम आज भी ज्ञात नहीं हो सका है। इसमें एकं तोता अपने स्वामी के परदेस चले जाने पर उसकी पत्नी को ये कथाएँ सुनाकर उसके चरित्र की रक्षा करता है।
सिंहासन द्वात्रिंशतिका –
इस ग्रन्थ में सङ्कलित 32 कथाओं को राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में लगी 32 पुतलियाँ राजा भोज को सुनाती हैं। इसके लेखक और रचनाकाल दोनों ही ज्ञात नहीं हैं।
**इन कथाओं के अतिरिक्त मैथिल कवि विद्यापति रचित ‘पुरुषपरीक्षा’; शिवदास-रचित ‘कथार्णव’ और बल्लालसेन-रचित ‘भोजप्रबन्ध’ नामक प्रसिद्ध कथासंग्रह हैं। इनमें ‘कथार्णव’ में 35 तथा ‘पुरुषपरीक्षा’ में 44 कथाएँ सङ्कलित हैं। ‘भोजप्रवन्ध’ में भिन्न-भिन्न काल के विभिन्न कवियों की कथाएँ सङ्कलित हैं। इनमें राजा भोज को दानशीलता, कवित्वप्रियता आदि का अत्युक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है।
जैन दन्त-कथाओं के रूप सिद्धर्षि द्वारा रचित ‘उपमितिभवप्रपञ्च कथा’; हेमचन्द्र द्वारा रचित ‘परिशिष्टपर्वन’ तथा आर्यशूर द्वारा रचित ‘जातकमाला’ भी संस्कृत के प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ हैं। ‘जातकमाला’ में महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित कथाएँ सङ्कलित हैं।
संस्कृत नाट्य-साहित्य का उद्भव और विकास :-
सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- (क) श्रव्य काव्य, (ख) दृश्य काव्य।
श्रव्य काव्य के अन्तर्गत वे सब रचनाएँ आती है जिसे पढ़कर आनन्दानुभूति की जाती है और दृश्य काव्य के अन्तर्गत नाट्य-साहित्य आता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य की अपेक्षा अधिक रमणीय एवं लोकप्रिय होता है। जिसको देखकर आनन्दानुभूति होती है। नाट्यशास्त्र साहित्य के प्रणेता भरतमुनि ने ‘पश्चम वेद’ की संज्ञा दी है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही सम्भवतः ‘काव्येषु नाटकं रम्यम्’ कहकर इसको समस्त साहित्यिक विधाओं के शिरमौर के रूप में विद्वानों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई है।
नाटक का उद्भव –
संस्कृत की अन्य विधाओं की भांति हमें संस्कृत नाट्य साहित्य के बीज वेदों में मिलते हैं। वहां स्थित यम- यमी संवाद नाट्य साहित्य का ही रूप है। इसके साथ ही ‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ ग्रन्थों में भी ‘नट’ ‘नाटक’ ‘रंग’ तथा ‘नर्तक’ आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है. जिसमे स्पष्ट होता है कि उसे समय नाटक पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध थे ।
संस्कृत का प्रथम नाटक –
संस्कृत का प्रथम नाटक रूप में 500 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि द्वारा रचित ‘जाम्बवतीजय’ को माना जाता है। यह नाटक आज प्राप्त नहीं है। इसके बाद 150 ईसा पूर्व सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतञ्जलि ने ‘कंस वध’ एवं ‘बालि-वध’ नामक दो नाटकों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। उपलब्ध नाटकों की दृष्टि से महाकवि भास संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जात है।
महाकवि भास –
महाकवि भास ने तेरह नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार है-
(१) बालचरितम्
(२) पंचरात्रम्
(३) कर्णभारम्
(४) दूतवाक्यम्
(५) दूतघटोत्कचम्
(६) उरूभंगम्
(७) मध्यमव्यायोगः
(८) अभिषेक नाटकम्
(९) अविमारकरम्
(१०) प्रतिमानाटकम
(११) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्
(१२) स्वप्नवासवदताम्
(१३) चारूदत्तम्
इनका समय ईसा पूर्व चौथी या पाँचवीं शती माना जाता है।
महाकवि कालिदास –
भास के पश्वात् संस्कृत नाट्य-साहित्य में महाकवि कालिदासः ने ‘मालविकाग्निमित्रम्’, विक्रमोर्वशीयम् तथा , ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ नामक तीन नाटकों की रचना की। इनमें ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इस विषय में यह उक्ति प्रचलित है-
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।
तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयम् ॥
महाकवि कालिदास का स्थितिकाल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है।
शूद्रक –
महाकवि शूद्रक-रचित एकमात्र नाट्यकृति ‘मृच्छकटिकम्’ को संस्कृत की श्रेष्ठ नाट्यकृति माना जाता है। समय 100 से 500 ईसवी के आस-पास निर्धारित किया जाता है।
विशाखदत्त –
ईसा की चौथी अथवा पाँचवीं शती में विशाखदत्त ने राजनीतिशास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य चाणक्य को कूटनीतिक कुशलता को प्रदर्शित करनेवाले नाटक ‘मुद्राराक्षसम्’ की रचना की। यह इनकी एकमात्र नाट्यकृति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई स्त्री पात्र नहीं है।
श्रीहर्षदेव –
सुप्रसिद्ध सम्म्राट् हर्षवर्धन के रूप में प्रतिष्ठित श्रीहर्षदेव ने तीन नाटकों की रचना की- ‘प्रियदर्शिका’, ‘रत्नावली’ और ‘नागानन्दम्’। इनकी ‘प्रियदर्शिका’ तथा ‘रत्नावली’ दोनों ही कृतियाँ श्रृंगार रसप्रधान है। ‘नागानन्दम्’ बौद्ध प्रेरित कृति है। श्रीहर्षदेव का स्थितिकाल छठी शताब्दी का पूर्वार्द्ध है।
भवभूति –
अपनी नाट्यकृतियों के द्वारा करुण रस को प्रतिष्ठित करनेवाले भवभूति ने ‘महावीरचरितम्’, ‘मालतीमाधवम्’ तथा ‘उत्तररामचरितम्’ नामक तीन श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। भगवान् राम के चरित्र पर आधारित ‘उत्तररामचरितम्’ इनकी श्रेष्ठ नाट्यकृति है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्कृत का एकमात्र ऐसा नाटक है, जिसमें करुण-रस की प्रधानता है। भवभूति का स्थितिकाल 700 ईसवी के लगभग माना जाता है।
भट्टनारायण –
ईसा की सातवीं शती के उत्तरार्द्ध में भट्टनारायण रचित ‘वेणीसंहारम्’ संस्कृत का एकमात्र दुःखान्त नाटक है। इसमें भीमसेन द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के बालों को गीला करके वेणी बँधने की कथा वर्णित है।
मूरारि –
वाल्मीकि ‘रामायण’ की कथा पर आधृत ‘अनर्घराघवम्’ मुरारि की प्रसिद्ध नाट्यकृति है। मुरारि का स्थितिकाल आठवीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है।
शीलभद्र –
जगद्गुरु शंकराचार्य के शिष्य शीलभद्र ने 800 ईसवी के लगभग अद्भुत रस में ‘आचार्य चूडामणि’ नामक नाटक की रचना की।
कृष्णमिश्र –
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग कृष्णमिश्रजी ने ‘सुबोध-चन्द्रोदय’ नाटक की रचना की। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है।
उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त दामोदर मिश्र द्वारा रचित हनुमन्नाटकम्ः क्षेमेश्वर द्वारा रचित ‘नेषधानन्दम्’ एवं ‘चण्डौशिक : राजशेखर द्वारा रचित बालसभा द्वारा रचित हनुमन्नाटकम, क्षेमेश्वर मात्रिका’ और ‘कर्पूरमञ्जरी’; जयदेव द्वारा रचित ‘प्रसन्नराघवम्’; दिङ्नाग द्वारा रचित ‘कुन्द्रमाला’ ‘एवं, वत्सराज द्वारा रचित ‘समुद्र-मन्थन’ संस्कृत की सुसिद्ध नाट्य-कृतियाँ हैं।
निवेदन – यदि आप कोई इस पोस्ट से सबंधित सुझाव देना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।
हमें फॉलो करना ना भूलें ।