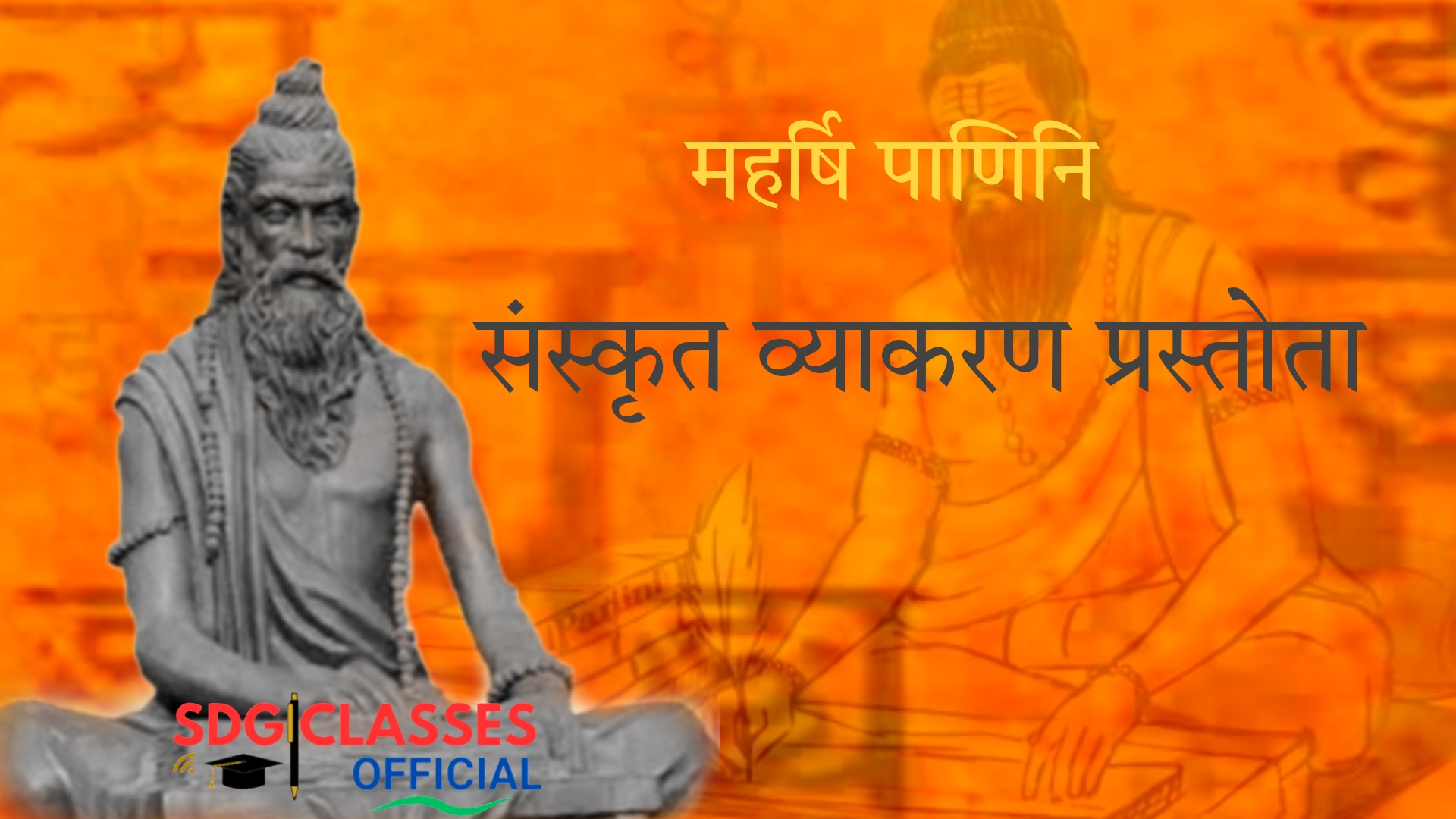संज्ञा प्रकरण संस्कृत– Sanskrit Sandhi
सम्प्रसारण संज्ञा
सूत्र—इग्यणः सम्प्रसारणम् ( 1/1/45 )
सूत्रार्थ—यण् का अर्थात् य,र,ल,व के स्थान पर इक् अर्थात् इ,उ,ऋ,लृ हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है ।
जहाँ-जहाँ भी सम्प्रसारण का उच्चारण हो , वहाँ-वहाँ यण् के स्थान पर इक् होना समझा जाय। संज्ञा प्रकरण संस्कृत-Sanskrit Sandhi का उदाहरण निम्न है।
उदाहरण—
वद् धातु मे व का सम्प्रसारण होकर उक्त बना।
यज् धातु का इष्ट।
वह् धातु का उढ़।
टि संज्ञा
सूत्र– अचोऽन्त्यादि टि ( 1/1/64 )
सूत्रार्थ—यह सूत्र टि संज्ञा करने वाला है । यह सूत्र टि संज्ञक वर्णों को बताता है ।
अचः अन्त्य आदि टि ।
किसी भी शब्द के अन्तिम से आदि अच् वर्ण की टि संज्ञा होती है। या
किसी भी शब्दों के अन्तिम स्वर और यदि उसके तुरंत बाद कोई व्यञ्जन हो तो वह भी टि संज्ञा कहा जाता है,
उदाहरण—
राजन् में अन् टि है ।
मनस् में अस् टि है ।
शक में क का अकार टि है ।
उपधा संज्ञा
सूत्र—अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा ( 1/1/65 )
संज्ञा प्रकरण संस्कृत-Sanskrit Sandhi सूत्र प्रकार- यह सूत्र उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है। जो उपधा संज्ञक वर्णों को बताता है।
सूत्रार्थ—अलः अन्त्यात् पूर्व उपधा संज्ञा स्यात्।
वर्णों के किसी भी समुदाय में से जो अन्तिम वर्ण हो, उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होती है।
उदाहरण—
राम में अन्त्य वर्ण है मकार के बाद का अकार और उससे पूर्व का वर्ण है मकार, अतः मकार की उपधा संज्ञा होगी।
र्+आ+म्+अ में अ से पूर्व वर्ण म् की उपधा संज्ञा होगी ।
इसी तरह आदित्य में यकार की उपधा संज्ञा होगी ।
श्याम में मकार की उपधा संज्ञा होगी ।
प्रतिपादिक संज्ञा
सूत्र- अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ( 1/2/45 )
सूत्र प्रकार- यह सूत्र प्रातपदिक संज्ञा सूत्र करने वाला है।
सूत्रार्थ—धातु , प्रत्यय और प्रत्ययान्त के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान् शब्द स्वरूप प्रातपदिक संज्ञक होता है।
प्रातिपदिकसंज्ञा के लिए अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् और कृत्तद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा करने वाले दो ही सूत्र हैं । प्रातिपदिकसंज्ञा इसलिए जरूरी है कि जो सुप् आदि ये प्रातिपदिक संज्ञक शब्दों से होते हैं । प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं होगी तो सुप् आदि प्रत्यय भी नहीं होंगे ।
इनके अतिरिक्त कृदन्त, तद्धितान्त और समस्त पदों की भी यह संज्ञा प्राप्त होती है—कृत्तद्धितसमासाश्च सूत्र द्वारा ।
उदाहरण—राम शब्द लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम मात्र होने से यह अर्थवान् है, उसके विषय में न यह धातु है और न ही प्रत्ययान्त है। इसलिए यह प्रातपदिक कहा जायेगा ।
पद संज्ञा
सूत्र—सुप्तिङ्न्तं पदम् ( 1/4/14 )
सूत्र प्रकार- यह सूत्र पद संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ- सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्।
सुबन्त और तिङन्त पदसंज्ञक होते हैं । जिन शब्दों में सु,औ,जस् आदि सु से लेकर सुप् तक के प्रत्यय जिन शब्दों में लगे हुए हो, उन शब्दों को सुबन्त कहते हैं ।
और तिप्, तस्, झि आदि से महिङ् तक के प्रत्यय जिन शब्दों के अन्त में लगें हो उन्हें तिङन्त कहते हैं ।
सुबन्त और तिङन्त की पद संज्ञा इस सूत्र से की जाती है । पद संज्ञा करने पर ही वे पद कहलाते हैं । पद होने के बाद ही वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है ।
अपदं न प्रयुञ्जीत अर्थात् जो पद नहीं है, वह लोक में व्यवहार के योग्य नहीं होता है ।
राम + सु = रामः
पठ् + तिप् = पठति
भ संज्ञा
सूत्र—यचि भम् ( 1/4/18 )
सूत्र प्रकार- यह सूत्र भ संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ- य् च, अच् च यच्।
सु आदि से लेकर कप् तक के प्रत्ययों में यकार और स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्दों की पद संज्ञा न होकर भ संज्ञा होगी ।
घु संज्ञा
सूत्र—दाधाध्वदाप् ( 1/1/20 )
सूत्र प्रकार- यह सूत्र घु संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ – दा – स्वरूप वाले तथा धा – स्वरूप वाले धातुओं की घुसंज्ञा होती है, दाप् ( काटना) और दैप् ( साफ करना ) धातुओं को छोड़कर ।
जो धातु स्वयं दा और धा के रूप में आदेश होती हैं ऐसी धातुओं की घुसंज्ञा कर दी जाती है ।
घ संज्ञा
सूत्र—तरप्तमपौ घः ( 1/1/23 )
सूत्र प्रकार—यह सूत्र घ संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ– तरप् और तमप् इन दो प्रत्ययों की घसंज्ञा होती है।
जब दो लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ तरप् प्रत्यय लगाया जाता है ।
और जब बहुत लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ तमप् प्रत्यय लगाया जाता है।
विभाषा संज्ञा
सूत्र प्रकार—यह सूत्र विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ– जहाँ विकल्प से होने और न होने, दोनों की स्थिति बनी रहती है वहाँ विभाषा संज्ञा होती है ।
निष्ठा संज्ञा
सूत्र—क्तक्तवतू निष्ठा ( 1/1/26 )
सूत्र प्रकार— यह सूत्र निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ—क्त और क्तवतु इन दोनों प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है ।
यह प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय हैं ।
संयोग संज्ञा
सूत्र—हलोऽनन्तराः संयोगः ( 1/1/7 )
सूत्र प्रकार—यह सूत्र संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ—हलः अनन्तराः संयोगसंज्ञाः स्युः।
हल् अर्थात् व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर के न रहने पर, उन सभी हलों के समुदाय की संयोग संज्ञा होती है ।
जैसे- देवदत्त , भव्य, आदित्य आदि। यहाँ पर दत्त में दो तकार है, दोनों के बीच में कोई अच् अर्थात् स्वर वर्ण नहीं है। इसलिए त्-त् हल समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाती है ।
संहिता संज्ञा
सूत्र—परः सन्निकर्षः संहिता ( 1/4/109 )
सूत्र प्रकार— यह सूत्र संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ—वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्।
वर्णों की अत्यन्त निकटता ( समीपता ) को संहिता कहते हैं । जिसकी संहिता संज्ञा नहीं हुई होती, उसमें सन्धि नहीं हो सकती ।
जैसे – श्याम + अवतार में श्याम के मकार का अकार और अवतार के अकार में अत्यंत समीप है । इसलिए दोनों अकारों की आपस में संहिता संज्ञा हो गयी ।
प्रगृह्य संज्ञा
सूत्र— ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् ( 1/1/11 )
सूत्र प्रकार—यह सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है ।
सूत्रार्थ—ईत् , ऊत् , एत् अर्थात् ईकारानत, ऊकारान्त और एकारान्त ( ई, ऊ, ए ) द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती हैं ।
जैसे- हरी एतौ, विष्णू इमौ, पचेते इति आदि।
सत् संज्ञा
सूत्र—तौ सत् ( 3/2/127 )
सूत्र प्रकार—यह सूत्र सत् संज्ञा करने वाला सूत्र है।
सूत्रार्थ—शतृ और शानच् प्रत्यय की सत् संज्ञा होती है।
सवर्ण संज्ञा
सूत्र—तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् ( 1/1/9 )
सूत्र प्रकार—यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है।
सूत्रार्थ—जिन दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान तथा आभ्यान्तर प्रयत्न दोनों समान हों, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है ।
जैसे- अ-आ, इ-ई, उ-
ऊ, आपस में सवर्णी है ।
लता + अपि = लतापि।
हरि + ईशः = हरीशः ।
वधु + उत्सवः = वधूत्सवः।
पितृ + ऋणम् = पितॄणम्।